मृत्यु के भय का गीता में वैज्ञानिक विवेचन
By पं. नरेंद्र शर्मा
आत्मा की अमरता और मृत्यु के अधीनता का रहस्य
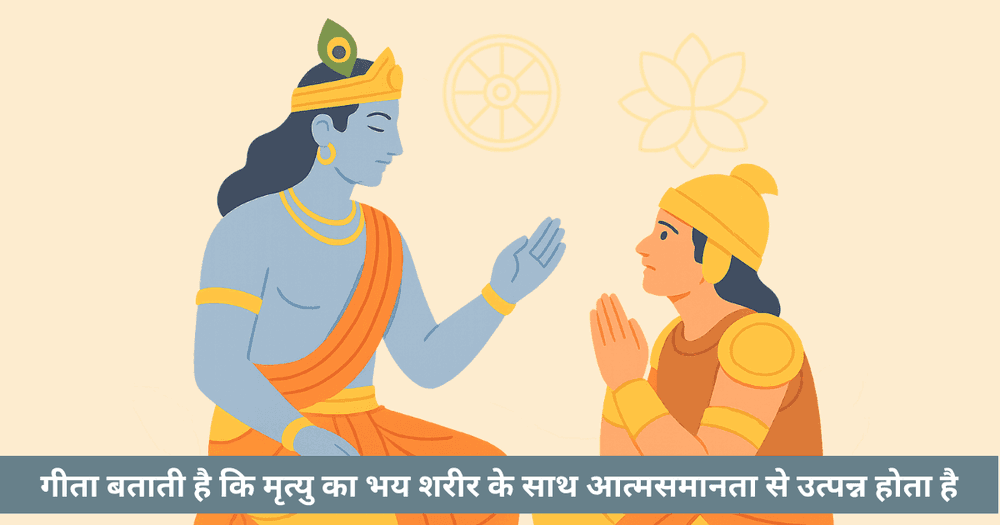
सामग्री तालिका
मृत्यु का भय शायद मनुष्य का सबसे गहरा मानसिक बोझ है। यह हमारे भीतर इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हम शरीर को ही आत्मा का स्वरूप मान बैठते हैं, अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझ लेते हैं और अज्ञान के कारण अपनी अमर आत्मा को भूल जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता इस विषय में अद्भुत मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने स्पष्ट किया कि मृत्यु का भय केवल भ्रांति और मोह है। यदि आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध हो जाए तो मृत्यु का विचार भी शांति और स्वीकार्यता के साथ ग्रहण किया जा सकता है।
शरीर को आत्मा मानने की भ्रांति
गीता बताती है कि मृत्यु का भय सबसे पहले शरीर के साथ आत्मसमानता से उत्पन्न होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है और समय के प्रवाह में क्षीण होता चला जाता है। किंतु आत्मा शाश्वत है, जिसे न अस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जब हम आत्मा और शरीर का भेद भूल जाते हैंतब मृत्यु को अंत समझकर भयभीत हो उठते हैं। वस्तुतः मृत्यु आत्मा के लिए वस्त्र परिवर्तन मात्र है, न कि अस्तित्व का लोप।
मोह और आसक्ति का बंधन
पारिवारिक स्नेह, धन-संपत्ति और प्रतिष्ठा-ये सब मनुष्य को मोहग्रस्त कर देते हैं। गीता इस अवस्था को मोह कहती है, अर्थात् अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेना। मृत्यु जब इन बंधनों को तोड़ती है तब भय उत्पन्न होता है। किंतु जो व्यक्ति भलीभाँति जान लेता है कि इनका स्वामित्व केवल क्षणिक है, वही मृत्यु का सामना शांति के साथ कर सकता है और आत्मिक आनंद में स्थिर रह सकता है।
अहंकार और नियंत्रण का भ्रम
मनुष्य का अहंकार यह मानता है कि वह अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। योजना बनाना, संचय करना और सुरक्षित रखना, इन सबके पीछे अहंकार की छाया है। मृत्यु उस भ्रम को एक झटके में तोड़ देती है। गीता का उपदेश है कि यह अहंकार ही माया है। यह समझते ही साधक जान लेता है कि वह कभी वास्तविक नियंत्रणकर्ता था ही नहीं। जब नियंत्रण का भ्रम मिट जाता है, मृत्यु का भय भी मिटने लगता है।
आत्मा के शाश्वत स्वरूप को भूलना
गीता के अनुसार भय का मूल कारण आत्मा की अमरता को न जान पाना है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह सदैव अनादि, अविनाशी और सर्वव्यापी है। किंतु जब मनुष्य शरीर और मन को ही अपना सब कुछ मान लेता हैतब मृत्यु को संहार मान बैठता है। आत्मा की शाश्वतता को अनुभव कर लेने पर मृत्यु केवल एक यात्रा की कड़ी बन जाती है, जिसमें चेतना आगे बढ़ती है।
अपूर्ण इच्छाओं का बोझ
अधूरी इच्छाएँ और अपूर्ण कामनाएँ मृत्यु के समय मनुष्य को सबसे अधिक अस्थिर कर देती हैं। गीता बताती है कि कामनाएँ ही आत्मा को बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में बाँधती हैं। जितनी कामनाएँ भारी होती हैं, मृत्यु का भय उतना ही तीव्र होता है। आत्मशुद्धि, त्याग और निष्काम कर्म के द्वारा इच्छाओं का परिशोधन संभव है। इससे मृत्यु का क्षण सहर्ष स्वीकार्य बन जाता है।
साधना की स्थिरता का अभाव
केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में साधना के रूप में उतारना भी आवश्यक है। श्रीकृष्ण ने स्थितप्रज्ञ की स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें साधक सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीवन-मृत्यु में समान रहता है। ध्यान, भक्ति, तप और सेवा जैसे अभ्यास आत्मा की स्थिरता को पुष्ट करते हैं। बिना साधना और अनुशासन के मृत्यु के समय ज्ञान भी डगमगा जाता है और भय हावी हो जाता है।
मृत्यु के भय से परे जाने का मार्ग
गीता व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त हो सकती है।
- ज्ञानयोग: आत्मा की अमरता को बार-बार स्मरण कर जीवन का दृष्टिकोण बदलना।
- कर्मयोग: निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना और फल का त्याग करना।
- भक्तियोग: ईश्वरीय शरण में रहकर अहंकार का समर्पण करना।
- ध्यानयोग: मन को बार-बार स्थिर कर सत्य में एकाग्र करना।
इन योगों का अभ्यास मृत्यु की शंका को समाप्त करता है। तब मृत्यु वस्त्र परिवर्तन की भाँति सहज दिखाई देने लगती है।
अर्जुन का भय और कृष्ण का उपदेश
कुरुक्षेत्र में अर्जुन मृत्यु के भय से विचलित होकर शस्त्र विहीन हो गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप का उद्घाटन किया। उन्होंने मृत्यु को समाप्ति न बताकर केवल संक्रमण की अवस्था कही। गीता का यह उपदेश आज भी प्रत्येक खोजी आत्मा के लिए दीपक बनकर मार्गदर्शन करता है।
आत्मबोध का सजीव संदेश
जब कभी भीतर मृत्यु का भय जागृत हो, उसी क्षण यह स्मरण करना चाहिए कि हम न शरीर हैं, न मन हैं। हम चिरस्थायी आत्मा हैं, समय के साक्षी और शाश्वत सत्ताएँ। इस अनुभूति के साथ जीवन निडर बन सकता है। तब न प्रेम में आसक्ति रहती है और न मृत्यु में भय। आत्मा न कभी जन्मी है और न कभी नष्ट हो सकती है। यही गीता का परम सत्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मृत्यु का भय गीता के अनुसार क्यों उत्पन्न होता है?
उत्तर: मृत्यु का भय शरीर को आत्मा समझने, मोहग्रस्तता, अहंकार और आत्मा की अमरता के अज्ञान से उत्पन्न होता है।
प्रश्न 2: गीता में आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है?
उत्तर: आत्मा अमर, अजर, अविनाशी और शाश्वत है, जो शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है।
प्रश्न 3: मृत्यु का भय कम करने के लिए कौन-कौन से योग गीता में बताए गए हैं?
उत्तर: ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ध्यानयोग मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए गीता में सुझाए गए हैं।
प्रश्न 4: मोह और अहंकार मृत्यु के भय को कैसे बढ़ाते हैं?
उत्तर: मोह अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मानने से और अहंकार नियंत्रण का भ्रम बनाए रखने से भय बढ़ता है।
प्रश्न 5: स्थिरप्रज्ञ का अर्थ क्या है और इसका मृत्यु के भय से क्या संबंध है?
उत्तर: स्थिरप्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सुख-दुख और जीवन-मृत्यु की दुःखद घटनाओं में भी स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति भय से मुक्त रहता है।
पाएं अपनी सटीक कुंडली
कुंडली बनाएंक्या आपको यह पसंद आया?
लेखक

पं. नरेंद्र शर्मा (63)
अनुभव: 20
इनसे पूछें: पारिवारिक मामले, करियर
इनके क्लाइंट: पंज., हरि., दि.
इस लेख को परिवार और मित्रों के साथ साझा करें