कृष्ण सभी को तुरंत क्यों नहीं बचाते? कर्म, प्रेम और मुक्ति की गूढ़ता
By पं. संजीव शर्मा
कर्म का विधान, स्वतंत्रता, लीला, मुक्ति, भागवत दर्शन, FAQs
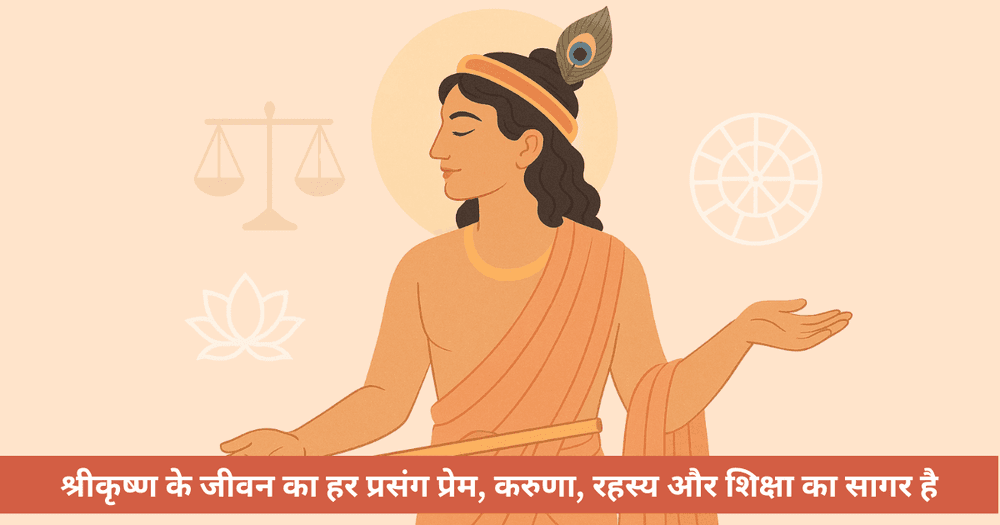
सामग्री तालिका
श्रीकृष्ण के जीवन का हर प्रसंग शाश्वत प्रेम, करुणा, रहस्य और शिक्षा का सागर है। गोकुल की गलियों में माखन चुराते नटखट बाल, कालिय नाग को अधीन करते अद्वितीय योद्धा, द्रौपदी के वस्त्रहरण पर अनायास प्रकट होने वाला रक्षक, कुरुक्षेत्र में विपन्न अर्जुन के सम्मुख संपूर्ण जगत का स्वामी-यह सब श्रीकृष्ण के विभिन्न आयाम हैं। इन सब से भी बड़ा उनका वह जिम्मेदार मौन है, जब वे चाह कर भी सभी को तात्कालिक संकटों से नहीं बचाते। प्रश्न सहज घुमता है-जब कृष्ण सर्वशक्तिमान और दयालु हैं तब वे सभी का दुःख क्यों नहीं हर लेते? क्यों कुछ लोग भीषण पीड़ा में, संघर्ष या अकेलेपन में, पूरे जीवन कठिनाई झेलते हैं?
यह प्रश्न केवल भक्तों का नहीं बल्कि वेद, दर्शन, कर्म सिद्धांत और भगवद्गीता के जिज्ञासु सम्प्रदायों में भी बार-बार आता है। इसका उत्तरा सतही नजरिए से नहीं, गहरे वैदिक और आध्यात्मिक विश्लेषण से मिलता है: श्रीकृष्ण कभी आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म के फल और प्रेम की चेतना के नियमों को नहीं तोड़ते। वे राह दिखाते हैं, सहारा देते हैं-पर अनुभव करने, आगे बढ़ने और जागरूक होने का अधिकार जीवात्मा को ही सौंंपते हैं।
कौन-कौन से सिद्धांत श्रीकृष्ण के व्यवहार को दिशा देते हैं?
1. ‘जैसा भाव, वैसी कृपा’- भगवद्गीता का मार्गदर्शक सूत्र
श्रीमद्भगवद्गीता (4.11) में श्रीकृष्ण कहते हैं, ‘‘यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्।’’ अर्थात, जो जैसी भावना, श्रद्धा और ईमानदारी से मेरे पास आता है, मेरी कृपा उसी रूप में उस तक पहुँचती है। कोई संसार चाहता है, कोई मोक्ष, कोई केवल कृष्ण-हर दिशा में अनुग्रह उसी अनुरूप मिलता है।
यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है; चाहे पारिवारिक जीवन की सुख-शांति हो, करियर में लक्ष्य, या साधना-योग का पथ। श्रीकृष्ण कभी भी किसी की आकांक्षा, कर्म अथवा प्रेम की सीमा से बाहर अपनी कृपा को आरोपित नहीं करते।
2. कर्म का फल अपरिहार्य है- ईश्वर भी नियम से बंधे हैं
महाभारत में, गांधारी अपने पुत्रों के विनाश पर श्रीकृष्ण से आर्त प्रश्न करती हैं। तब श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं-‘कर्मफल के विधान में कोई अपवाद नहीं होता। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी उस नियम का उल्लंघन नहीं करते।’
यदि हर कर्म के परिणाम स्वतः मिटा दिए जाएं, तो जीवन का अर्थ, शिक्षा, अनुभव और प्रगति-सब खो जाएगा। कर्म जीवात्मा को सीखाने, परिपक्व करने और आत्म-ज्ञान की दिशा में अग्रसर करने का साधन है।
| कर्म के प्रकार | परिणाम | वृद्धि का मार्ग |
|---|---|---|
| सत्कर्म (धर्म/सत्य) | शांति, सुख, समाज में उन्नति | सकारात्मक संस्कार |
| दुष्कर्म (अहं/अधर्म) | दुख, बाधा, विपरीत शिक्षा | आत्म-सुधार, जागृति |
3. स्वतंत्र चिन्तन और विकल्प: आत्मिक विकास का मूल
भगवद्गीता (18.63) में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- ‘‘ज्ञान भी दिया, रहस्य भी; अब स्वयं सोचो और निर्णय लो।’’
स्वतंत्रता ईश्वर का वास्तविक उपहार है। वे किसी को बाध्य नहीं करते। श्रीकृष्ण किसी भी साधक, परिवार, या समाज को अपनी स्थिति बदलने, न बदलने, या स्वयं अपने अनुभव से सीखने की ‘पूर्ण आज़ादी’ देते हैं। प्रेम और भक्ति का मूल्य तभी है, जब वह निर्बाध, स्वेच्छा से अपनाई जाए।
| जीवन क्षेत्र | स्वतन्त्रता का प्रभाव | मार्गदर्शन |
|---|---|---|
| आध्यात्मिक | साधना, भक्ति का चयन | इच्छा का सम्मान |
| व्यावहारिक | निर्णय, जिम्मेदारी | अनुशासन व सुधार |
| पारिवारिक | संबंधों में खुलापन, समर्पण | विश्वास व संवाद |
4. लीला: अनुभव से शिक्षा, तात्कालिक उद्धार नहीं
श्रीकृष्ण के सभी कार्य ‘लीला’-अर्थात् मुक्त, प्रेममय, उद्देश्यपूर्ण खेल-हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिय नाग के विषहरण, युद्ध का निर्णायक होना-हर घटना में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक धरातल पर बड़ा सन्देश है:
- सहजता में धर्म, अनुशासन में प्रेम, विपत्ति में धैर्य
- लीला केवल तात्कालिक समस्या समाधान नहीं, दीर्घकालीन चेतना विस्तार का माध्यम है
यदि हमेशा तत्काल रक्षा, अवरोध-मुक्ति या पीड़ा मेटा दी जाए, जीवन में संघर्ष, शिक्षा, आत्मनिष्ठा और जीवात्मा का परिपक्व अनुभव खो जाएगा।
5. मुक्ति: आज्ञा नहीं, संबंध और प्रेम का उदात्त बंधन
भागवत पुराण में मार्मिक रूप से वर्णन है-श्रीकृष्ण के लिए ‘मुक्ति’ संघर्ष, पीड़ा से भागना नहीं बल्कि भक्ति का जीवंत संबंध बनाना है। यशोदा की डोरी में वे बंध जाते हैं, द्रौपदी के आंसुओं में वे उमड़ते हैं, गोपियों के विरह में वे स्वयम् टूट जाते हैं।
ईश्वर चाहता है कि साधक अपने प्रेम, कर्म और समर्पण के प्रत्येक भाव में उसे निकट अनुभव करे। हर बाधा में साथ, हर संघर्ष में प्रोत्साहन, हर विजय में अहंकार से मुक्ति-यही सच्चा ‘कृष्णानुभव’ है।
क्या हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा पा सकता है?
हर आत्मा में स्वतंत्रता, चैतन्य और करुणा की चेतना बोयी गयी है। श्रीकृष्ण ‘मुक्ति’ का द्वार हर आत्मा के लिए खोलते हैं, लेकिन प्रवेश की चाबी स्वयं साधक के पास है। उनका सबसे बड़ा वरदान है-प्यार, कर्म, सुधार, रिश्तों का अविरल प्रवाह; वह कभी शक्तिमान आदेश नहीं बनता बल्कि हर जीव के साथ निजी संवाद, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और आत्मानुभूति के रूप में आता है।
FAQs: श्रीकृष्ण, कर्म, मुक्ति और लीला पर प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण
प्रश्न 1: अगर श्रीकृष्ण चाहें तो हर किसी का दुःख क्यों नहीं मिटा देते?
उत्तरा: जीवन का उद्देश्य अनुभव, शिक्षा और आत्म-परिवर्तन है; पीड़ा और संघर्ष भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना सुख। श्रीकृष्ण मार्ग दिखाते हैं, लेकिन स्वीकृति और प्रयास साधक के हाथ में होता है।
प्रश्न 2: क्या भगवान हमारे कर्मफल को बदल नहीं सकते?
उत्तरा: वे नियम और कर्मफल के सनातन सिद्धांत को नहीं तोड़ते। हाँ, प्रेम व प्रकट समर्पण के साथ, भगवान अनुकूलता और शक्ति ज़रूर देते हैं।
प्रश्न 3: अर्जुन को भी श्रीकृष्ण ने केवल उपदेश ही क्यों दिया? जबरन क्यों नहीं सुधारा?
उत्तरा: भक्ति और ज्ञान का असली स्वरूप तभी उन्नत होता है, जब वह खुद की चाहत, अनुभव और सोच से स्वीकारा जाए-अन्यथा वह केवल दिखावा बनके रह जाता है।
प्रश्न 4: श्रीकृष्ण की लीला का आज के जीवन में क्या उपयोग है?
उत्तरा: लीला का अर्थ है-हर क्षण को प्रेम, जागरूकता और लगातार सुधार के साथ जीना। संघर्ष को कठिनाई न मानकर, शिक्षा व संबंध का माध्यम बनाना।
प्रश्न 5: क्या अंतिम समय पर हर आत्मा भगवान की कृपा पा सकती है?
उत्तरा: हाँ, जब जीव सच्चे भाव, प्रेम और समर्पण से पुकारता है, श्रीकृष्ण सदा हृदय में उतर आते हैं। यह वचन पूरे भागवत-दर्शन का मूल है।
श्रीकृष्ण का व्यवहार प्रेम, कर्म, स्वतंत्रता और शिक्षा में संतुलन का प्रतिबिंब है। वे मार्गदर्शक हैं, नियंत्रक नहीं; रक्षक हैं, प्रवर्तक नहीं। उनका जीवन और संदेश बार-बार यही सिखाता है-हर आत्मा अपनी यात्रा, कर्म, रिश्ता और मुक्ति का मार्ग खुद खोजे। ईश्वर साथ है, हमेशा; पर प्रेम, कर्म और जागरूकता के साथ ही मिलते हैं।
पाएं अपनी सटीक कुंडली
पाएं अपनी सटीक कुंडलीक्या आपको यह पसंद आया?
लेखक

पं. संजीव शर्मा (50)
अनुभव: 15
इनसे पूछें: पारिवारिक मामले, आध्यात्मिकता और कर्म
इनके क्लाइंट: दि., उ.प्र., म.हा.
इस लेख को परिवार और मित्रों के साथ साझा करें